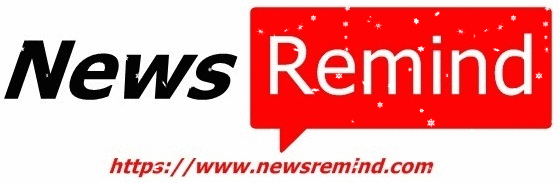अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नेताओं के शब्दों और उनके वास्तविक कदमों में फर्क आम बात है, लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपने राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। हालिया घटनाएँ इसका स्पष्ट उदाहरण हैं। एक तरफ़ ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को “घनिष्ठ मित्र” बताते हुए भारत-अमेरिका रिश्तों को “असीम संभावनाओं वाली साझेदारी” बताते हैं और जल्द ही व्यापार समझौते की उम्मीद जताते हैं। वहीं दूसरी ओर वे यूरोपियन यूनियन से अपील करते हैं कि भारत और चीन पर 100% टैरिफ़ लगाकर रूस को कमजोर किया जाए।
यह विरोधाभास यूं ही नहीं है, बल्कि ट्रंप की रणनीति का हिस्सा है। वे अमेरिकी मतदाताओं के बीच खुद को “सख्त नेता” के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। रूस पर दबाव बनाने के लिए ऊँचे आयात शुल्क की बात कर वे यह संदेश देते हैं कि भारत और चीन को भी मजबूर किया जा सकता है कि वे रूसी तेल पर निर्भरता कम करें। चुनावी माहौल में यह छवि उन्हें घरेलू राजनीति में फ़ायदा पहुँचाती है।
ट्रंप की डिप्लोमेसी का यही पैटर्न है—एक ओर दोस्ताना भाषा और दूसरी ओर दबाव की धमकी। भारत को “प्राकृतिक साझेदार” कहना और साथ ही ऊँचे टैरिफ़ की चेतावनी देना इसी रणनीति का हिस्सा है। उनका मकसद भारत को यह एहसास कराना है कि यदि वह अमेरिकी हितों के मुताबिक़ नहीं चला तो आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी।
अब सवाल यह है कि यूरोप ट्रंप की बात मानकर भारत पर टैरिफ लगाएगा या नहीं? हकीकत यह है कि यूरोपियन यूनियन भारत के साथ इस साल के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) करना चाहता है। यूरोपीय देशों के लिए भारत एक तेज़ी से बढ़ता बड़ा बाज़ार है, जिसे खोने का जोखिम वे नहीं उठा सकते। यूक्रेन युद्ध ने यूरोप को यह सिखाया है कि एकतरफा निर्भरता खतरनाक होती है। इसलिए अब वह एशियाई साझेदारों को संतुलित करने की नीति पर चल रहा है और इस दृष्टि से भारत उसके लिए बेहद अहम है।
यूरोप यह भी जानता है कि ट्रंप के बयानों में स्थिरता नहीं होती। जो आज “करीबी मित्र” हैं, वे कल “बड़े प्रतिद्वंद्वी” भी कहे जा सकते हैं। इसलिए यूरोप के लिए ट्रंप की सलाह मानकर जल्दबाज़ी में फैसला लेना अपने दीर्घकालिक हितों के खिलाफ़ होगा।
स्पष्ट है कि ट्रंप की शैली “दोहरी रणनीति” पर टिकी है—एक ओर मधुर शब्द और दूसरी ओर कड़े कदमों की धमकी। यह तरीका उन्हें घरेलू राजनीति में तो लाभ देता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। यूरोपियन यूनियन इस बात से वाक़िफ़ है और रूस को लेकर उनकी नाराज़गी होने के बावजूद भारत के साथ बढ़ते आर्थिक रिश्ते अधिक प्राथमिकता रखते हैं। इसलिए यूरोप का भारत पर टैरिफ़ लगाने की संभावना बहुत कम है।
भारत के लिए यह स्थिति अवसर बनकर आई है। वह यूरोप के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को मज़बूती दे सकता है और साथ ही अमेरिका के साथ संवाद बनाए रख सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक ट्रंप की बयानबाज़ी को संतुलित दृष्टिकोण से देखा है। वे जानते हैं कि ट्रंप की धमकियाँ अक्सर वार्ता की मेज़ पर दबाव बनाने के लिए होती हैं, न कि वास्तविक नीति का हिस्सा। इसलिए मोदी ने भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय संयम और धैर्य का रास्ता चुना है।
मोदी की यही रणनीतिक शांति उनकी कूटनीति की सबसे बड़ी ताक़त है। वे समझते हैं कि अंतरराष्ट्रीय रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, बल्कि लंबे समय तक निभाए गए व्यवहार से तय होते हैं। यही कारण है कि अमेरिका दबाव डालने के बावजूद भारत जैसे बड़े और उभरते साझेदार पर कठोर कदम नहीं उठा पाएगा। तर्क और संयम से आगे बढ़ने वाली यही नीति भारत को आने वाले समय में और मजबूत वैश्विक स्थिति दिलाएगी।