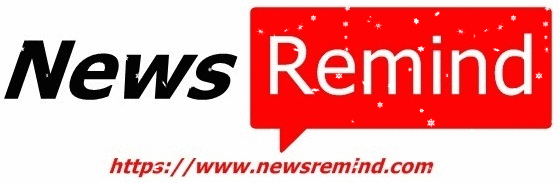भारत का ई-कचरा एक बड़ा आर्थिक अवसर प्रदान कर रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में धातु निष्कर्षण के माध्यम से प्राप्त सामग्री से 6 बिलियन डॉलर (₹520,674,000,000) कमाने की क्षमता है। भारत अब चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कचरा उत्पादक है। RedSeer Strategy Consultants की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरीकरण और बढ़ती आय के कारण देश का ई-कचरा वित्त वर्ष 2014 में 2 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) से दोगुना होकर वित्त वर्ष 2024 में 3.8 MMT हो जाएगा।
मुख्य रूप से घरों और व्यवसायों द्वारा उत्पन्न उपभोक्ता खंड ने वित्त वर्ष 2024 में कुल ई-कचरे में लगभग 70 प्रतिशत का योगदान दिया। ई-कचरे के उत्पादन में एक प्रमुख प्रवृत्ति सामग्री की तीव्रता में बदलाव है। जबकि उपकरण अधिक कॉम्पैक्ट और हल्के होते जा रहे हैं, त्यागे गए सामानों की मात्रा बढ़ रही है, जिससे कुशल रीसाइक्लिंग रणनीतियों की आवश्यकता होती है।
भारत के लिए बड़ा अवसर-
रेडसीर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स के पार्टनर जसबीर एस. जुनेजा ने कहा, “आने वाले वर्षों में ई-कचरे की मात्रा बढ़ने की उम्मीद है। ई-कचरे में धातुओं का बढ़ता मूल्य भारत के लिए रिकवरी दक्षता बढ़ाने और खुद को संधारणीय धातु निष्कर्षण में अग्रणी के रूप में स्थापित करने का एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है।” वर्तमान में, भारत में उपभोक्ता ई-कचरे का केवल 16 प्रतिशत औपचारिक रीसाइक्लर द्वारा संसाधित किया जाता है। वित्त वर्ष 25 तक औपचारिक रीसाइक्लिंग क्षेत्र में 17 प्रतिशत सीएजीआर वृद्धि के अनुमानों के बावजूद, यह भारत के केवल 40 प्रतिशत ई-कचरे को संभालने की उम्मीद है।
इस क्षेत्र को अनौपचारिक खिलाड़ियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जो कम अनुपालन लागत और व्यापक संग्रह नेटवर्क से लाभान्वित होते हैं। इस बीच, 10-15 प्रतिशत ई-कचरा घरों में ही जमा रहता है और 8-10 प्रतिशत लैंडफिल में चला जाता है, जिससे रीसाइक्लिंग दक्षता कम हो जाती है। एक स्थायी ई-कचरा प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए, भारत सरकार ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) ढांचा पेश किया है। तब से EPR उत्पादकों के लिए परिभाषित संग्रह लक्ष्यों के साथ एक अनिवार्य प्रणाली में विकसित हो गया है। हालांकि, कम न्यूनतम EPR शुल्क और अपर्याप्त औपचारिक रीसाइक्लिंग क्षमता के कारण अंतराल बने हुए हैं।
धातु आयात कम हो सकता है-
औपचारिक रीसाइक्लिंग नेटवर्क को मजबूत करना धातु वसूली दरों में सुधार और रिटर्न को अधिकतम करने की कुंजी है। इससे भारत की धातु आयात मांग में 1.7 बिलियन डॉलर तक की कमी आ सकती है, जबकि उच्च मूल्य वाली पुनर्नवीनीकरण धातुओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सकती है।